हर रोज लगभग २२५ लाख लोग हमारी रेलगाड़ियों में यात्रा करते हैं। इनमें कोई १६० लाख लोग लंबी दूरी के यात्री होते हैं। भारतीय रेल की दस हजार से...
हर रोज लगभग २२५ लाख लोग हमारी रेलगाड़ियों में यात्रा करते हैं। इनमें कोई १६० लाख लोग लंबी दूरी के यात्री होते हैं। भारतीय रेल की दस हजार से ज्यादा रेलगाड़ियां हर रोज चलती हैं पूरे देश भर में। करीबन सात हजार से ज्यादा स्टेशन और ५२,००० से अधिक सवारी डिब्बों में देश का एक हिस्सा दूसरे हिस्सों से परिचित होता है। इन डिब्बों में कई जबानें बोली जाती हैं, भांति-भांति का खाना-पीना, रहनसहन, कपड़ा-लत्ता होता है। तरह-तरह के लोग एक-दूसरे से टकराते हैं। कोई एक लाख किलोमीटर से अधिक लंबाई है रेल पटरियों की, यानी धरती से चांद तक एक पंक्ति में लगा दो तो कोई एक-तिहाई रास्ता नापा जा सके।
बहुत सी जमीन भी है रेलवे के पास। ११ लाख एकड़ से ज्यादा। गोआ राज्य की कुल जमीन से भी सवाई ज्यादा। इसमें से कई हजार एकड़ तो यूं ही खाली पड़ी रहती है। इतनी जमीन की रखवाली करना कतई आसान नहीं है। वैसे तो हमारे यहां सरकारी जमीन पर कब्जे होते ही रहते हैं, पर रेलवे की जमीन हथियाना खासा आसान होता है। ऐसी ही जमीन उन लोगों का आसरा होती है जो मुसीबत में गांवों और छोटे शहरों को छोड़ कर बड़े शहरों में पहुंचते हैं, रोजगार, सुविधा और बेहतर भविष्य की आशा में। लेकिन उन्हें वे सुविधाएं नहीं मिल पातीं जो उनके पहले आ बसे लोगों को मिली हुई होती हैं। हमारी शहरी आबादी का ज्यादातर हिस्सा दो-चार पीढी पहले गांवों या छोटे शहरों में रहता था। हर शहर की कहानी में कई तरह के शरणार्थी आते हैं।
पुराने शरणार्थी नए शरणार्थियों को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि सीमित साधनों पर आबादी का दबाव बढ़ जाता है। नए शरणार्थियों को जैसी भी परिस्थिति मिले उसे स्वीकार करना पड़ता है। बड़े शहरों में रोजगार आसानी से मिलता है, सो रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हो जाता है। लेकिन शहरों में मकान आसानी से नहीं मिलते। ज्यादातर नए लोगों को जैसे-तैसे कर के झोपड़पट्टियों में या दूसरे तंग इलाकों में थोड़ी सी जगह मिलती है। सिर पर छत होना जरूरी होता है, घर में शौचालय के होने का सवाल बाद में आता है। वैसे भी गांव से आए लोगों को तो खुले में शौच जाने की आदत होती है, उन्हें यह उतना अटपटा नहीं लगता। पर घनी आबादी वाले शहरों में खुली जगह मिलना आसान नहीं होता। रेलवे की जमीन ऐसे में बहुत काम आती है। पटरियों के इर्दगिर्द शौच निपटते लोग आम बात है। यह दृश्य शहरों के भीतर और आसपास ज्यादा दिखता है। कई जगहों पर तो लोगों के पास शौच जाने की जगह एकदम ही नहीं होती। ऐसे में रेल पटरी के ठीक ऊपर बैठने के सिवा कोई उपाय नहीं होता। रेलवे अधिकारी मानते हैं कि देश भर में कुल पटरी की जमीन का एक प्रतिशत ऐसा है जिस पर घनघोर मलत्याग होता है। कुछ लोगों ने तो भारतीय रेल को एक बहुत बड़े शौचालय की उपमा भी दी है। एक पटरी पर चलती रेलगाड़ी में बैठे लोग खिड़की से झांकते हुए दूसरी पटरी पर मलत्याग करते लोगों को देखते हैं। कभी-कभी तो बगल की पटरी पर चलती रेलगाड़ी के जाने तक लोग खड़े हो कर अपनी लज्जा ढंक लेते हैं, कभी बैठे-बैठे ही केवल मुंह फेर लेते हैं। अगर ऐसा रोजाना करना पड़े तो लोगों को इस शर्मिंदगी की आद्त पड़ जाती है। रेलगाड़ी के यात्री भी ऐसे दृश्यों के आदी हो जाते हैं। महिलाओं के लिए तो यह और भी अपमानजनक होता है। मलत्याग करना आखिर शरीर का दैनिक धर्म ठहरा, सो खींच कर बैठ जाती हैं। इन इलाकों में महिलाएं आमतौर से सूरज उगने के पहले शौच निपटने जाती हैं या अंधेरा होने के बाद। अंधेरे में गरिमा तो थोड़ी बचती है, लेकिन जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों और जानवरों से खतरा हमेशा रहता है। इसके कारण एक और बड़ा खतरा खड्डा हो जाता है: रेल दुर्घटना का। पानी और मल-मूत्र में ऐसे रसायन होते हैं जो धीरे-धीरे इस्पात को गला देते हैं। इसका असर पड़ता है उन कब्जों पर जो पटरी को नीचे बिछे स्लीपर से बांध कर रखते हैं। इन कब्जों को अगर समय-समय पर बदला न जाए तो दुर्घटना का डर बढ़ता जाता है। रेलवे को हर साल इन गले हुए कब्जों को बदलने पर ३००-५०० करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। कई और तरह के दैनिक हादसे होते हैं जिनकी चर्चा नहीं होती। पटरी के रखरखाव का काम करने वाले रेलवे कर्मचारी मल-मूल और उसकी बदबू के बीच में अपना काम करते हैं। रेलवे को लगभग डेढ लाख सफाई कर्मचारी रखने पड़ते हैं, जिनका एक खास काम होता है पटरी से मल-मूत्र साफ करना। लेकिन इनमें से बहुत कम को पक्का रोजगार मिलता है। ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर होते हैं जो किसी ठेकेदार के लिए काम करते हैं। पटरी और स्लीपर से सूखा मल छुड़ाना आसान नहीं होता। उसे पानी, झाडू और हाथ की मेहनत ही हटा पाती है।
यह काम कुछ खास जाति और समाज के लोग करते हैं, जिन्हें आए दिन अपमान और अन्याय झेलना पड़ता है। न्यायालयों में हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर आए दिन अभियोग चलते रहते हैं। आए दिन रेलवे अधिकारियों को न्यायालय आड़े हाथों लेता है, क्योंकि हाथ से मैला ढोने का काम करवाना गैरकानूनी है।
पटरी से लेकर न्यायालय की मेज तक फैली इन विषमताओं का आदर्श समाधान है शौच निपटने की कोई और व्यवस्था। पर निकट भविष्य में तो हर किसी को शौचालय मुहैया होना नामुमकिन है। कई सालों की भरसक और लगातार कोशिशों के बाद भी ऐसा होना आसान नहीं होगा, चाहे इसमें कितने ही हजार करोड़ रुपये डाल दिए जाएं। अगर पटरी के ऊपर और आसपास लोगों का मलत्याग करना बंद हो भी जाए तो भी पटरियों पर मल-मूत्र गिरता ही रहेगा क्योंकि इसका एक और स्रोत है: रेलगाड़ी के भीतर बैठे यात्री। वे चाहे खिड़की से बाहर झाँकते हुए खुले में शौच जाने वालों को नीची नजर से देखें, लेकिन सवारी डिब्बों के दोनों ओर बने शौचालयों की नालियां उनके ठीक नीचे खुलती हैं। खुले में पटरी पर मलत्याग तो केवल घनी आबादी वाली बस्तियों में ही होता है, जबकि रेलगाड़ी के शौचालयों के जरिए मलमूत्र पूरे देश भर में पटरी के ऊपर गिरता है।
तेज चलती रेलगाड़ी के नीचे हवा से मल- मूत्र पटरी के ऊपर और आसपास बिखर जाता है। हवा इतनी तेज होती है कि मल पिछले डिब्बे के नीचे चिपक जाता है। डिब्बी: के रखरखाव करने वाले कारीगरों का इस गंदगी से सामना तो होता ही है, डिब्बों का इस्पात भी कमजोर पड्ता है। रेलगाड़ी के शौचालयों से निकला पानी धीरे-धीरे डिब्बे का निचला हिस्सा गलाता है। ऐसे डिब्बों की मरम्मत पर रेलवे का खर्चा भी ज्यादा होता है। अगर हर रोज १६० लाख लोग लंबी दूरी की रेलगाड़ी में सफर करते हैं और एक दिन में औसतन एक मनुष्य २०० से ४०० ग्राम मल पैदा करता है, तो २० लाख से ४० लाख किलो मल हर रोज पटरियों पर यात्रियों द्वारा गिराया जाता है। जो कोई भी रेलगाड़ी में शौच जाता है वह हाथ से मैला साफ करवाने की कुरीति को बढ़ावा तो देता ही है, पटरी और उसके कब्जों को गलाने में भी हाथ बंटाता है। क्या पता, भविष्य में होने वाली किसी रेल दुर्घटना में वह छोटा सा योगदान भी दे रहा हो। इसका मूल कारण है डिब्बों में बने शौचालयों की नाली की बनावट। इसे बदलने की कोशिशें लगभग ४० साल से रेलवे में चल रही हैं। जैसे एक प्रस्ताव आया था कि इन नालियों का मुंह दोनों पटरियों के बीच में खोला जाए, बजाए पटरी और कब्जों के ठीक ऊपर। लेकिन यह बनावट चली नहीं। मल नाली के मोड़ में चिपक कर तेज हवा से सूख जाता था। उसे साफ करना और भी मुश्किल हो जाता। नाली सीधी हो या मुड़ी हुई, स्टेशन पर खड़ी गाड़ियों के शौचालयों से निकलने वाला मल-मूत्र पटरी पर ही गिरता है। वहां से उठ कर मक्खियां प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों पर बैठती हैं। _
वैसे शौचालयों में लिखा होता है कि स्टेशन पर खड़ी गाड़ी में उसका इस्तेमाल चाहिए। लेकिन मल-मूत्र को त्यागने की जरूरत शौचालय पर लिखे नोटिस लोग स्टेशन पर खड़ी गाड़ी में भी शौचालय जाते ही हैं, जिसका नतीजा नीचे गिरता है। इसे साफ करने के लिए रेलवे को ढेर सारे पानी की व्यवस्था करनी पड्ती है, स्टेशन की पटरी पर 'एप्रन' लगाने पड़ते हैं, जो मैले पानी को बहा कर एक निश्चित नाली के जरिए सीवर में डाल दें। हर एक प्लेटफॉर्म पर लगने वाले एप्रन की कीमत २ करोड़ रुपये होती है। इनमें मैला बहाने के लिए अथाह पानी चाहिए होता है जिसके लिए हर कहीं रेलवे को ट्यूबवेल डालने पड़ते हैं। पानी की किल्लत तो हमारे सभी शहरों में रहती ही है। ऐसे में स्टेशन साफ रखना बहुत कठिन होता है, जो किसी भी स्टेशन पर देखा जा सकता है। इस सब में हम कैसे फंस गए? भारतीय रेल की समस्या दूसरे देशों में चलने वाली रेलगाड़ियों से एकदम अलग है। दूसरे देशों में लोग मलत्याग करने के बाद कागज का इस्तेमाल करते हैं, पानी का नहीं। उन देशों के रेल डिब्बों में बने शौचालयों के नीचे एक टंकी बनी होती है जिसमें मैला इकट्ठा होता है। इसे किसी मुनासिब जगह पर खाली किया जाता है, जहां से मैला सीवर में पहुंचता है। हवाई जहाजों में भी ऐसी ही व्यवस्था होती है। पर हमारे यहां पानी इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से मल-मूत्र के साथ ढेर सारा पानी भी शौचालय की नाली में बहाया जाता है। भारतीय रेल ने भी ऐसे टैंक आजमाए। लेकिन उनसे केवल स्टेशन पर मैला गिरना रुका, क्योंकि इन टंकियों को चलती रेल में खोलना पड़ता था। मैला पानी फिर भी पटरी पर ही गिरता, उसके कब्जों को गलाता, हवा के साथ फैल कर डिब्बों के नीचे चिपकाता। रेलगाड़ी के डिब्बों के नीचे बहुत बड़ी टंकी लगाने की जगह नहीं होती है। फिर इतनी बड़ी टंकी को भी साफ तो करना ही पड़ता। तमाम तरह के इंजीनियरी के समाधान रेलवे ने आजमाए लेकिन फिर भी समस्या जस-की-तस बनी रही। फिर एक समाधान निकला, लेकिन वह सिविल इंजीनियरी से नहीं, जीवविज्ञान से आया। उसके पीछे थी २० साल की साधना, जिसे सेना के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वैज्ञानिकों ने किया था। इस संगठन को डी.आर.डी.ओ. भी कहते हैं। सेना को इस काम में क्यों जुटना पड़ा ? जवाब है सियाचिन में तैनात सैनिकों की परेशानी के कारण। सन् १९८४ में भारतीय सेना ने एक सैनिक टुकडी सियाचिन के हिमनद पर तैनात की थी। जमी हुई बर्फ के इस वीराने में जीवन बहुत मुश्किल होता है। इतनी ठंड में ॐ मल सडु कर गलता नहीं है, बर्फ के साथ ही जमा रहता है। मल को गलाने वाले बैक्टीरिया इतने कम तापमान पर जीवित ही नहीं रहते। यही कारण है कि सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट के आसपास पर्वतारोहियों के मल-मूत्र की व प्रदूषण हो रहा है। सियाचिन में इससे एक और समस्या आती थी। सैनिक उसी हिमनद पर . करते थे जो उनका एकमात्र जल स्रोत था, और जहां की बर्फ गला कर _ मिलता था। सेना को जरूरत थी ऐसे शौचालयों की जो इतनी मुश्किल कर सकें, पर आकार में छोटे हों और इस्तेमाल में आसान। यह काम डी.आर.डी. ओ. को सौंपा गया। सन् १९८९ में जीववैज्ञानिक लोकेंद्र सिंह इस काम में जुट गए।
ठंड में काम करने वाले तरह-तरह के जीवाणुओं के साथ वे सालों-साल प्रयोग करते रहे। उसमें अंटार्कटिका महाद्वीप की ठंड में जीने वाले बैक्टीरिया की खोज से भी मदद मिली। श्री लोकेंद्र और उनके सहयोगियों को समझ आ गया कि समाधान उन्हीं बैक्टीरिया में मिलेगा जो बिना ऑक्सीजन के जीते हैं। श्री लोकेंद्र और उनके सहयोगियों ने ऐसे कई जीवाणुओं को कई सालों तक पाला, उन्हें मुश्किल हालात में जीने लायक बनाया। कुछ वैसे ही जैसे लोग अपने पालतू जानवरों को करतब सिखाते हैं। इन जीवाणुओं को ऑक्सीजन रहित टंकियों में रख कर हिमालय के पार बसे लद्दाख प्रांत में आजमाया गया।
कई सालों के परीक्षण और विफलताओं के बाद समझ में आया कि किस तरह के जीवाणु क्या करते हैं और उनसे काम कैसे लेना है। यह भी कि इन्हें ठीक काम करने के लिए किस तरह की टंकियां चाहिए। इनमें ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पानी के इस्तेमाल से मल को अपना भोजन बना लेते हैं और अम्ल की खटाई के रूप में उसे निष्कासित करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो इन तेजाबों को गला कर सिरका बना लेते हैं, और ऐसे भी जो इस सिरके को गला कर उससे पोषण लेते हैं और बचे हुए मैल को प्राकृतिक गैस बना देते हैं।
कुछ इसी प्रकार के बैक्टीरिया हमारे पेट में भी बसते हैं, और उनके बिना हम भोजन पचा नहीं सकते। यही कारण है कि मल के साथ हमारी आंत से पाद के रूप में प्राकृतिक गैस भी निकलती है। लेकिन हमारे पेट के तापमान की तुलना सियाचिन की बर्फ से नहीं हो सकती। कई वर्षों के परीक्षण से डी.आर.डी.ओ. ने वहां की कठोर परिस्थिति में कारगर एक 'बायोडाइजेस्टर' शौचालय बना लिया था। इसके भीतर जाता है मनुष्य का मल और मूत्र, बाहर केवल पानी आता है और प्राकृतिक गैस। जिस समय इस शौचालय की रूप-रेखा तैयार हो चुकी थी उसी समय रेलवे अपने यात्री डिब्बों के शौचालय बदलने के परीक्षण कर रहा था। इसके पहले जो कुछ आजमाया गया था वह काम नहीं आ रहा था। ऐसे में डी.आर. डी.ओ. के शौचालय भी लगा कर देखे गए। शुरूआती अनुभव हालांकि कड़वे ही थे। डी.आर.डी.ओ. रक्षा मंत्रालय की संस्था है और उसका काम गुप्त रहता है। रेलवे _ भी एक सरकारी संस्थान जरूर है, पर है एकदम सार्वजनिक। दोनों में तालमेल धीरे _ धीरे बढ़ा। इस साझेदारी में उन लोगों का पत्ता कटा जो दूसरे तरह के शौचालय रेलवे को बेच कर उनके रखरखाव का ठेका भी चाहते थे। बायोडाइजेस्टर शौचालय में उनकी मुनाफाखोरी की गुंजाइश नहीं थी, सो रेलवे के परीक्षणों में कई तरह के रोड़े डाले गए। लेकिन रेलवे में कुछ अधिकारियों को समझ आ चुका था कि उनके लिए कारगर समाधान तो यही है। सो रेलवे ने ऐसे शौचालय रेलगाड़ी के सवारी डिब्बों में लगाना शुरू किया है। रेल के डिब्बों में काम करने के लिए डी.आर.डी.ओ. के बनाए ढांचों में कुछ फेरबदल भी की गई। खासकर सूखे कचरे को टंकी में जाने से रोकने के लिए, क्योंकि यात्रियों को पुराने शौचालयों में हर तरह की चीजें फेंकने की आदत है। इसमें बोतल और पान मसाले के प्लास्टिक से ले कर शिशुओं के पोतड्रे भी आते हैं। इन्हें रोकने के लिए शौचालय के छेद के नीचे विशेष छलनी बनाई गई है।
सन् २०१६ के फरवरी महीने तक १०,००० से अधिक डिब्बों में ३२,००० से ज्यादा शौचालयों को बायोडाइजेस्टर में बदल दिया गया है। शुरू में हर डिब्बे के चार में से दो शौचालयों को ही बदला जा रहा है क्योंकि ऐसे शौचालय लगाना आसान नहीं है। हर डिब्बे में चार शौचालय लगाने की लागत है कोई चार लाख रुपये। सारे सवारी डिब्बों में बायोडाइजेस्टर शौचालय लगाने का खर्चा आज की कीमत पर कोई २,००० करोड़ रुपये होगा। सभी सवारी डिब्बों में शौचालय बदलने में आठ से दस साल लग जाएंगे। डिब्बों को रेलगाड़ियों से निकाल कर कारखाने में लाने से रेलवे के संचालन पर असर पड़ता है। फिर भी, रेलवे के कई अधिकारी अब इस पद्वति में पूरा विश्वास रखते हैं। धीरे-धीरे ही सही, लेकिन उन्हें भरोसा है कि रेलवे अपने डिब्बों की गंदगी मिटा सकेगा। कुछ अधिकारी तो इस असंभव काम को संभव कर दिखाने के लिए डी.आर.डी.ओ. के श्री लोकेंद्र को जादूगर पुकारते हैं। भारत में रेल आने के १५० साल बाद शौचालय की एक व्यावहारिक रूपरेखा तैयार हुई है। शुचिता का विचार आया है। क्या ऐसा जादू हमारे शहरों और गांवों में हो सकता है? इसे समझने के लिए पहले रेलवे पर एक करीबी नजर डालिए। भारतीय रेल अकेली सरकारी संस्था है जिसका बजट अलग से बनता है और जिसके पास स्वशासित ढांचा है। रेलवे बोर्ड बहुत ताकतवर संस्था है जिसका भारत नियंत्रण है, जो उसे चलाती है, रेल मंत्री और कैबिनेट रेलवे को पास १३ लाख कर्मचारियों की सेना है, खास इंजीनियरिंग की पूरी फौज भी है। पिछले ४० सालों से रेलवे में कोशिशें बनाने की। इस कवायद में उसका साथ निभाया सेना पास शोध और विकास के लिए ढेर साधन हैं। अब जरा दृश्य बदलें। रेलवे और उसके विशाल सं अपनी गरीब और थकी हुई नगरपालिकाओं को कोई प्राथमिकता नहीं है। कुछेक बड़े शहरों को छोड़ दें तो हमारे बाकी सभी नगर निगम कंगाल हैं। जो थोड़ा धन होता है वह नागरिकों को पानी पहुंचाने और सड्क-पुल बनाने जैसी कोशिशों में लग जाता है, क्योंकि इन सुविधाओं की मांग बहुत भारी होती है। पीने के पानी की आपूर्ति और मैले पानी का निस्तार आम तौर से नगर निगम की एक ही संस्था करती है। केंद्रीय सरकार में भी पेयजल और स्वच्छता का काम एक ही मंत्रालय के पास है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी पानी और स्वच्छता की बात एक साथ की जाती है, एक ही संस्था में।
शासन के हर स्तर पर ज्यादातर पैसा और साधन पानी की आपूर्ति में खर्च होता है, मैले पानी को साफ करने पर नहीं। राजनेताओं की रुचि भी पानी के जुगाड़ में होती है क्योंकि इससे जनता को रिझाना आसान है। हर शहर की सुविधाओं की मांग अंत नहीं है। जितनी पानी की आपूर्ति बढ़ती है उतना ही मैला पानी भी बढ़ता है, क्योंकि जितना भी पानी किसी शहर में इस्तेमाल होता है उसका ८० फीसदी सीवर की नाली में पहुंचता है। पर मैले पानी के निस्तार और उसकी सफाई में किसी की भी गंभीर रुचि नहीं होती है। जब मुश्किल बहुत बढ़ जाती है तभी शहर का ध्यान मैले पानी या कचरे की ओर जाता है, लेकिन तब तक मुश्किल बूते से बाहर हो चुकी होती है। इस विषय में अनुभव और ज्ञान रखने वाले कहते हैं कि पानी मुहैय्या कराने में मुनाफा भी है और व्यापार के अवसर भी। वे याद दिलाते हैं कि हमारे घरों में पानी साफ करने की मशीनों और बोतलबंद पानी की बिक्री बेतहाशा बढ़ी है। बोतलबंद _ पानी के बाजार का मूल्य १०,००० करोड़ रुपये से ज्यादा आंका जा रहा है। पीने का पानी साफ करने वाली महंगी मशीनें बेचने वाली एक कंपनी ने इस बाजार का मूल्य सन् २०१३ में ३,२०० करोड़ रुपये बताया था। ये बाजार दो साल में दोगुना हो जाता है तरह अनियमित है। पानी साफ करने की मशीनों के लिए कोई मानक तय मनमानी करने के लिए आजाद है। ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है उतना ही ज्यादा मैला पानी सीवर की । मैला पानी साफ करने के लिए ऐसी कोई होड़ नहीं है जैसी पीने के पानी को जो नुकसान होता है वह अदृश्य रहता है। वी इमारतें बना ली हैं, बड़ी-बड़ी नदियों को बांध लिया है और अंतरिक्ष से ले कर सागर तक की गहराई नाप ली है। परिणामों की चिंता करना जीवन का स्वभाव नहीं है। प्राणी केवल अपने लिए अवसर तलाशते हैं। सहज ही एक तरह के जीव का कचरा दूसरे तरह के जीव का साधन बन जाता है। इसीलिए मनुष्य की बस्तियों के इर्दगिर्द सूअरों जैसे प्राणी न जाने कब से रहते आए हैं। उन्हें मनुष्य के मल में भोजन मिलता रहा है। गाय-बैल और घोडे जैसे जीवों को फसल की ठंढ में खाना मिलता है। उनके गोबर की खाद खेतों को उर्वर बनाती है। प्रकृति के इस सीधे से सिद्धांत को आधुनिक शहर नजरअंदाज करते हैं। घनी आबादी वाले शहरों में मनुष्य के सिवा दूसरे प्राणियों के रहने की जगह नहीं बचती। इसलिए घनी बस्ती से निकले मल-मूत्र का प्राकृतिक संस्कार नहीं हो पाता है। इसका समाधान यही है कि मैले पानी को नदियों और तालाबों में डाल दिया जाए। आधुनिक शहर जल स्रोतों से पानी निकालते हैं और मैला पानी उनमें वापस डाल देते हैं।
यह तभी होता है जब सभी शौचालय सीवर की नालियों से जुड़े हों। दुनिया के एक बड़े हिस्से में ऐसा भी नहीं होता। ज्यादातर तो फ्लश कमोड का मैला पानी किसी पक्के या कच्चे गड्डे में डाल दिया जाता है। जमीन के नीचे किसी अंधे कुएं में जाकर उसकी उर्वरता तो बेकार हो ही जाती है, भूजल भी दूषित होता है। यह प्रदूषण दिखता नहीं है। जो अदृश्य हो उसकी चिंता भी कम ही होती है। सीवर के मैले पानी से होने वाला जल प्रदूषण आमतौर पर आंखों से दूर रहता है। जो दिखाई देता है वह है सड़कों और खुले इलाकों के आसपास पड़ा मल, यहां-वहां खुले में मलत्याग करने बैठे लोग। हमारी सरकारों का ध्यान खुले में मलत्याग रोकने के लिए शौचालय बनाने में ज्यादा है, उन शौचालयों से होने वाले जल प्रदूषण की ओर एकदम नहीं है। पिछले कुछ सालों से केंद्र सरकार भरसक कोशिश कर रही है कि पूरे देश में खुले में मलत्याग बंद हो। इसके दो कारण हैं। जहां एक व्यक्ति का मल दूसरे व्यक्ति से सीधे संपर्क में आता है वहां जानलेवा बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं। चूंकि लोगों को मलत्याग करने फिर वहीं जा कर बैठना पड़ता है जहां कोई और बैठ कर गया हो, तो रोगाणुओं को नए शिकार आसानी से मिलते जाते हैं। हर नया बीमार रोगाणुओं के लिए कई और लोगों के संक्रमण का माध्यम बनता है। इनके सबसे आसान शिकार बच्चे होते हैं। इस गंदगी की कीमत कई रपटों और शोध ग्रंथों में बार-बार जताई जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की फरवरी २०३३ की ही एक रपट कहती है कि हमारे देश में हर साल १५ लाख से अधिक बच्चों की मौत दस्त वाले रोगों से होती है। इन बीमारियों के रोगाणु तभी फैलते हैं जब रोगियों के मल के कण किसी-न-किसी रास्ते होता हुआ नए लोगों के पानी या भोजन में पहुंच जाते हैं। हमारे १०० में से ४५ बच्चों के शरीर का विकास ठीक से नहीं हो पाता, जिसका सबसे बड़ा कारण है मल से जुड़ी गंदगी, और निर्मल पानी की किल्लत। बच्चों का शरीर दुर्बल और नाटा रह जाता है, जैसे कि वे कुपोषण के शिकार हों। दूषित पानी से फैलने वाले रोग हर साल तकरीबन चार करोड़ लोगों को बीमार करते हैं। यही नहीं, घनी आबादी में खुले में शौच जाना बहुत शर्म का सबब होता है। जब मलत्याग करने की हड़बड़ी हो तब लोग शहरी भीड़ से भागते हुए, एकांत ढूंढते फिरते हैं। इससे हर कहीं, रस्ते-बा-रस्ते मल पड़ा रहता है। हमारे शहरों के कुछ हिस्से तो इतने गंदे हैं कि वहां पैदल चलना घिन पैदा करता है। शहरों के ऐन बीच में कीड़ों और मक्खियों से अटे ऐसे इलाके मिलते हैं। इनके आसपास ही घनी बस्तियां भी होती हैं। अब तो गांवों में भी पहले जैसे खुले मैदान और चारागाह नहीं बचे जहां लोग शांति से शौच जा सकें। पहले गांवों में शामिलाती जमीन इस तरह के काम के लिए छोड़ने का रिवाज था, ऐसी जमीन जो उपजाऊ न हो। ग्रामीण समाज इस जमीन की रक्षा भी करता था। वहां जानवरों को चरने के लिए भी छोड़ा जाता था। पर अब जमीन की होड़ में इन पर कब्जे हो गए हैं और सरकारों ने भी ऐसी जमीन भूमिहीनों को जोतने के लिए बांटी है।
आबादी भी बढ़ी है। जहां अभी भी खुले में शौच जाने लायक जमीन खाली है उसे इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत हैं। ऐसे गांव मिलना अब कतई मुश्किल नहीं है जहां हर कहीं मल पड़ा मिलता है। वातावरण में मल-मूत्र की बदबू सदा ही रहती है। जहां पैदल चलने के लिए साफ पगडंडी तक नहीं मिलती। सड्क के किनारे ही नहीं, सड़क के ऊपर भी इतना मल पड़ा होता है कि गाड़ियों को भी चलने की जगह नहीं बचती। रोगाणुओं के लिए यही स्वर्ग होता है।
भारत सरकार के लिए यह बहुत शर्मिंदगी की बात है। अंतर्राष्टीय गोष्ठियों में इसे भारत का सबसे निंदनीय पहलू कहा जाता है। बताया जाता है कि भारत से कहीं ज्यादा गरीब देशों ने भी इस मामले में तरक्की की है। वह भी ऐसे समय जब सरकार _ भरसक कोशिश कर रही है कि भारत की छवि एक शक्तिशाली, महाबली राष्ट्र की हो, ' आर्थिक विकास हुआ है। पर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दस में से तीन [क खुले में ही शौच जाते हैं। सब जानते हैं कि असल में यह अंक कहीं जितने लोग खुले में मलत्याग करने जाते हैं उनमें आधे से साल के बाद एक सरकारी सर्वेक्षण से पता लगा कि अनुदान राशि लोगों के लिए पर्याप्त प्रेरणा नहीं थी शौचालय बनाने के लिए। एकांत में सुविधा से शौच जाने की बात करना जरूरी था। सन् १९९९ में सरकार ने कार्यक्रम का नाम बदल कर अंग्रेजी में 'टोटल सैनिटेशन कैंपेन'रख दिया, यानी संपूर्ण स्वच्छता अभियान। महत्वाकांक्षा की कमी भारत सरकार की कमजोरी कभी नहीं रही है।
अब यह शौचालय की आपूर्ति करने वाला कार्यक्रम भर नहीं बचा था। इसका जोर था पंचायतों के जरिए लोगों को जानकारी दे कर स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने पर, ताकि पीने के पानी और भोजन में वह रोगाणु न पहुंचे जो खुले में शौच जाने से फैलते हैं। पंचायतों के साथ भागीदारी में जनसंपर्क और जनसंचार के लिए अलग से बजट रखा गया, ताकि जनसाधारण को शौचालय बनाने की जरूरत महसूस हो, लोग खुद से शौचालय बनाएं। सरकारी अनुदान केवल गरीब तबकों के लिए था। कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए कई नए पहलू जोड़े गए। सरकार ने जताया कि स्वच्छता उसकी प्राथमिकता है। सन् २०११ में केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता विभाग को मंत्रालय का दर्जा दिया गया। सन् २०१२-१३ में इसका बजट १४,००० करोड़ रुपये से ज्यादा था। इसी दौर में 'टोटल सैनिटेशन कैंपेन' का नाम बदल कर 'निर्मल भारत अभियान' कर दिया गया। सन् २०१४ में केंद्र में नई सरकार आने के बाद इस कार्यक्रम का नाम फिर बदला गया। अब इसे 'स्वच्छ भारत मिशन' कहते हैं। इन नामांतरणों के साथ ही कई _ नेताओं और मंत्रियों के झाडू चलाते हुए फोटो छपे। एक बार फिर सरकार ने खुले में मलत्याग को पूरी तरह खत्म करने का बीड़ा उठाया, सन् २०१९ तक। पुराने वादों को मिला एक नया नाम, एक नई तारीख। इन सब बदलावों के दौरान निर्मल ग्राम पुरस्कार' भी खूब चर्चित रहा। ग्राम पंचायतों को यह पुरस्कार तब दिया जाता है जब गांव में कोई भी खुले में मलत्याग करने नहीं जाता हो। जिस ग्राम पंचायत को यह पुरस्कार मिलता है उसकी प्रसिद्धि तो होती ही है, उसे कई तरह की विकास योजनाओं में प्राथमिकता मिलती है।
आशय है ग्राम पंचायतों में स्वच्छता को बढ़ावा देना। सन् २००३ से २०१३ तक २८,००० से ज्यादा गांव यह पुरस्कार पा चुके थे। केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का कहना था कि इस अभियान में पिछले दशक में ८.७ करोड़ से ज्यादा शौचालय बने। मतलब १२.५ करोड़ शौचालय बनाने के उसके लक्ष्य का ७० प्रतिशत पूरा हो चुका था। इन चमकदार आंकड़ों के पीछे एक तरह की बदबू थी। इसका कारण तो सन् २०११ की जनगणना तक पहुंचेंगे, जिससे पता चला कि वास्तव में केवल ५.१६ करोड़ घरों में शौचालय थे। मंत्रालय के आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा खर्च की राशि से निकले थे, जबकि जनगणना घर-घर जा कर हुई थी। इसका अर्थ साफ था: जैसा दूसरी सरकारी योजनाओं में होता है कुछ वैसा ही हुआ था निर्मल भारत अभियान में भी। धन जिस काम पर खर्च हुआ था वह काम पूरा नहीं हुआ। शौचालय सरकारी कागजों में ज्यादा हैं, घरों में कम बने। निर्मल ग्राम पुरस्कार के आंकड़ों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सन् २००८ में एक सर्वे ने छह राज्यों के १६२ ऐसे गांवों का जायजा लिया जिन्हें कुछ समय पहले ही यह पुरस्कार मिला था। केवल छह गांव ऐसे निकले जिनमें कोई भी खुले में मलत्याग नहीं करता था। बाकी गांवों में एक तिहाई ऐसे थे जिनमें हर दस में से चार लोग खुले में शौच जाते थे। कर्नाटक राज्य में हुए एक सर्वे में भी ऐसी ही परेशानियां दिखीं। कई जगहों पर शौचालय बनने के बाद भी लोग उनका इस्तेमाल नहीं करते मिले। योजना आयोग ने सन् २०१३ में एक सर्वेक्षण जारी किया जिसमें लिखा था कि ७३ प्रतिशत ग्रामीण घरों से कम-से-कम एक व्यक्ति खुले में मलत्याग करने जाता है। सन् २०१४ में चालू हुए स्वच्छ भारत मिशन के आंकड़े अभी आए नहीं हैं। इसमें शौचालय बनवाने में केंद्र सरकार का हिस्सा कम किया गया है, राज्य सरकारों का हिस्सा बढ़ाया गया है। कॉरपोरेट जगत को यह काम उसकी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत करने के लिए कहा गया है। राज्य सरकारों को अपने हिसाब से कार्यक्रम को ढालने की आजादी भी दी गई है। कुछ शोधकर्ताओं ने इसकी कार्यकुशलता समझने की कोशिश की है। उनकी रपटें और जांच परिणाम यही इशारा करते हैं कि शौचालय बनाने के कार्यक्रमों की जो समस्याएं पहले थीं वही अभी भी बनी हुई हैं। सन् २०१४ में जारी हुई दो महत्वपूर्ण रपटें सरकारी स्वच्छता कार्यक्रमों के बारे में कुछ चिंताजनक तथ्य दिखलाती हैं। दोनों ही रपटें कई महीनों के शोध और परीक्षण पर आधारित हैं। एक शोध मंडली ने गांवों में यह पता करने के लिए सर्वेक्षण किए कि लोग शौचालय इस्तेमाल क्यों नहीं करते।
पता ये चला कि अगर हरेक घर में शौचालय बन जाए तो भी खुले में मलत्याग बंद नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग शौचालय का . इस्तेमाल पसंद ही नहीं करते। वे शौचालय को एक गंदा स्थान मानते हैं, और उन ऎ क ह हैं। ऐसे बहुत से लोग बनाए गड्ढों के भर जाने पर उन्हें साफ करवाने से डरते हैं। ऐसे लोग जिनके धर में शौचालय बना हुआ है, लेकिन वे फिर भी खुले में मलत्याग करना ही स्वच्छ मानते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि स्वच्छता अभियानों को लोगों का अन और फिर उसमें सकारात्मक अंतर लाने पर ध्यान देना होगा। शौचालय बनाना भऱ तो कोई समाधान नहीं होगा। इस तरह के कार्यक्रमों को प्रशासनिक जामे से बाहर आ कर सामाजिक रूप अपनाना होगा। दूसरी शोध मंडली ने ओडीशा में यह पता किया कि शौचालय बनाने से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा। उन्होंने भी यही पाया कि शौचालय बनाना और उसका इस्तेमाल करना दो एकदम अलग बातें हैं। यह भी कि केवल शौचालय के इस्तेमाल से उन बीमारियों का असर कम नहीं होता जो मल से फैलती हैं। इन बीमारियों की रोकथाम के लिए सफाई के और भी तरीके अपनाने पड़ते हैं। यानी सरकार शौचालय बना कर भी इस समस्या से हाथ नहीं धो सकती है। दोनों ही शोध मंडलियों ने कोई क्रांतिकारी प्रयोग नहीं किए हैं। केवल गांव के लोगों से जा कर बात की है, उनसे उनका मन समझने की कोशिश की है। सन् १९८६ से चल रहे स्वच्छता अभियानों ने लोगों का मन टटोलने की कोशिश नहीं की, बस उन्हें गदा ठहराया और उनसे शौचालय का इस्तेमाल करने की बात बार-बार की। अपने ही लोगों के प्रति इस तरह की बेरुखी हमारे सरकारी तंत्र के मूल में है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो।
फिर हर सरकार यह बतलाती है कि उसने कितने शौचालय बनाने पर कितना धन खर्च किया है। अब तक सरकारी स्वच्छता अभियानों पर कई निष्पक्ष सर्वे और रपटें आ चुकी हैं। सभी सरकारी आंकड़ों का भुसभुसापन दिखलाती हैं। योजना आयोग की ही एक जरा पुरानी रपट कहती है कि स्वच्छता अभियान सरकारी मानसिकता का शिकार हैं। एक उद्देश्य जब तय हो जाता है, तो सब कुछ उसी के इर्दगिर्द घूमता है। लक्ष्य को पूरा हुआ दिखाने के लिए अगर सत्य की बलि देनी पड़े, तो दी जाती है। स्वच्छता कार्यक्रमों का उद्देश्य सीधा है, खुले में मलत्याग की प्रथा का अंत। आजकल बार-बार यह कहा जाता है कि शौचालयों के अभाव में महिलाओं को घर से दूर जाना पड़ता है और अपराध का खतरा झेलना पड़ता है। स्त्रियों और लड़कियों को असुविधा न हो यह बात तो स्वाभाविक है। लेकिन इस तरह की बात करने वालों के सामने कुछ सवाल उठते हैं। क्या शौचालय बनाने से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार बंद हो जाएगा? उसका संबंध पुरुषों के आचरण से है या महिलाओं के मलत्याग करने के स्थान से ? क्या घर में शौचालय बनने के बाद महिलाओं का घर से निकलना ही बंद हो जाएगा? क्या यह वांछनीय है? महिलाओं की सुरक्षा एक सामाजिक विषय है , इसका सीधा संबंध पुरुषों के व्यवहार से है, शौचालयों के स्थान से नहीं। ऐसा नहीं है कि सरकारी अभियानों में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। कई लोगों को सरकारी मदद और सुविधा मिली है। कुछ गांव सही में स्वच्छ हुए हैं। लेकिन यह भी दिखता है कि शुचिता का कार्यक्रम शौचालय बनाने की योजना बन कर रह गया है। शौचालय और शुचिता में अंतर है।
शौचालय बनाने भर से शुचिता नहीं आती, खासकर तब जब शौचालय से मैले पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक न हो। इसका उल्टा भी सही है। बिना शौचालय के भी शुचिता आ सकती है। अगर खुले में शौच जाने के लिए इतनी जमीन हो कि मल दूसरे लोगों के संपर्क में न आए और प्राकृतिक आड़ भी बनी रहे, तो इसे गंदगी फैलाने वाली व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। सरकार के काम में इतनी बारीकी की जगह नहीं होती है। सरकारी स्वभाव जिस भाषा में गढा जाता है वह अफसरी आदेश देने और उनका पालन करने के लिए होती है। सरकार के पास रिझाने या मन पर प्रभाव डालने वाली भाषा होती ही नहीं है। बहुत हुआ तो सरकारी भाषा में 'जनभागीदारी' जैसे शब्द आ जाते हैं। कार्यक्रम सरकार का ही रहता है, उसमें लोगों को भागीदारी भर देनी होती है, क्योंकि वे उन योजनाओं के 'लाभार्थी' और 'हितग्राही' होते हैं। सरकारी व्यवहार के केंद्र में हमेशा खुद सरकार ही होती है, लोग या उनका समाज नहीं। लोगों के सामाजिक कार्यक्रमों में सरकार की 'भागीदारी' के किस्से कम ही सुनने में आते हैं। फिर भी शिकायत यही की जाती है कि लोगों में सरकारी कार्यक्रमों के प्रति 'स्वामित्व' का भाव नहीं होता। इसी तरह के शब्द, इसी तरह की भाषा बहुत सी गैरसरकारी संस्थाओं में भी चलती है। इसलिए 'जनआंदोलनों' से ले कर 'जनसंस्थानों' में भी 'जनभागीदारी' की बात होती है। इसमें 'जन' केवल उपसर्ग भर रहता है, उसमें जन का मन टटोलने की कोशिश कम ही होती है। हमारे यहां शुचिता की तमाम आधुनिक बातचीत अंग्रेजी से आई है। इसका सीधा अनुवाद कर दिया जाता है। इस भाषा में साधारण लोगों के अनुभव और उनकी हकीकत की जगह नहीं होती। किसी भी दूसरी भाषा से शब्द या विचार लेना अच्छा ही होता है, भाषाओं का लेन-देन तो हमेशा से चलता रहा है। लेकिन अपनाए हुए शब्द और लादे गए शब्दों में फर्क होता है। 'साइकिल' और 'स्टाइल' भी अंग्रेजी से लिए हुए शब्द हैं, लेकिन इनका मतलब ज्यादातर लोगों को आज सहज पता है, ये अपनाए हुए शब्द हैं। ऐसा 'सैनिटेशन' के बारे में नहीं कह सकते हैं। यह भी अंग्रेजी का ही शब्द है। इसका भाव हिंदी में ठीक से बतलाना या इसका अनुवाद करना कठिन है। अंग्रेजी में भी यह कोई बहुत पुराना शब्द नहीं है। इसकी व्युत्पत्ति लातिन भाषा से है और अंग्रेजी में यह फ्रांसीसी भाषा से आया है। इसका आज के अर्थ में इस्तेमाल कोई १५० साल पहले ही शुरू हुआ जब यूरोप के घनघोर प्रदूषित शहरों की सफाई की बात होने लगी। - "सैनिटेशन'के अर्थ और भाव में केवल सफाई और स्वच्छता ही नहीं है, स्वास्थ्य और - मानसिक संतुलन भी है। जब किसी के व्यवहार में पागलपन झलके तो अंग्रेजी में कहा जाता है कि उसने अपनी 'सैनिटी' खो दी है। यह शब्द भी 'सैनिटेशन' के परिवार से ही है। एक पुराने शब्द ने नया भाव पकड़ा, नई समस्या से जूझने के लिए।
भारत सरकार को 'टोटल सैनिटेशन' का 'निर्मल भारत' करने में कुछ साल लगे। सन् २०११ में जब इसका पूरा मंत्रालय बना, तो उसका नाम अंग्रेजी में 'मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर ऐंड सैनिटेशन' रखा गया। लेकिन उसका हिंदी अनुवाद हुआ 'पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय'। स्वच्छता का मतलब केवल ऊपरी सफाई से है, 'सैनिटेशन' के अर्थ में नहीं, शुचिता या निर्मलता के अर्थ में नहीं।
शुचिता और निर्मलता पुराने, घिसे हुए शब्द हैं। ये हमारी कई भाषाओं के स्वभाव में मिले हुए हैं। आपको ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जिनका नाम निर्मल या शुचि या शुचिता हो। इसके भावार्थ में ऊपरी सफाई भी है और भीतरी पवित्रता भी। शुचिता तन की होती है और मन की भी। भ्रष्टाचार से घबराए लोग सार्वजनिक जीवन में शुचिता की मांग करते हैं। 'टॉएलेट' के लिए हिंदी में इस्तेमाल होने वाला शब्द 'शौचालय' आखिर शुचिता से ही निकलता है। लेकिन सरकार हो या गैरसरकारी संस्थाएं, शौचालय की जगह सबके दिमाग में है, शुचिता की जरा कम है।
यह केवल व्याकरण, शब्दकोष या भावार्थ की शास्त्रीय बहस भर नहीं है। हर शब्द में उसके पीछे के विचार, भाव और मूल्य भी झलकते हैं। शब्द बदल देने से या कोई और शब्द लगा देने से किसी व्यक्ति का विचार नहीं बदल जाता, व्यवहार बदलना तो बहुत दूर की बात है। 'टोटल सैनिटेशन' को 'निर्मल भारत' या 'स्वच्छ भारत' में बदलने से पूरा देश निर्मल और स्वच्छ हो जाएगा इसकी कोई जमानत नहीं है। इस सतही फेरबदल के पीछे का विचार शौचालय से निकला है, शुचिता से नहीं।
सरकारी स्वच्छता अभियान इसका सचित्र विवरण देते हैं। सरकारी मदद जिस तरह के शौचालय बनाने के लिए मिलती है उनकी रूपरेखा एक खाके से निकली हुई होती है। उनमें देश की विविधता की झलक नहीं होती, किसी भी स्थान की विशेष परिस्थिति की भी नहीं। निर्मल भारत अभियान में बने ऐसे शौचालय भी मिलते हैं जिनका मैल सोखने वाला गड्ढा किसी पानी के स्रोत से सट कर बना हो। देखते ही आभास हो जाता है कि ऐसे शौचालय रोगाणुओं का ही प्रसार करेंगे, शुचिता का नहीं, जबकि पानी के स्रोत से शौचालय की दूरी सरकारी नियमों में निश्चित है। यह भी दिख सकता है कि शौचालय के नीचे सेप्टिक टैंक ऐसी जगह बना है जहां जल स्तर बहुत ऊंचा है। अगर ऐसे शौचालय का उपयोग हो तो मल पानी में तैरता नजर आता है।
बहुत सी जगह शौचालय में पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। शौचालय बनाने का बजट तो सरकारी कार्यक्रम में है, लेकिन उसमें पानी पहुंचाने का बजट सरकार के पास है नहीं। कई जगह लोगों ने शौचालय बनवा लिए हैं लेकिन उनका उपयोग किसी साधारण कमरे या गोदाम की ही तरह करते हैं। अगर सरकार मुफ्त में चार दीवारें और एक छत बना कर दे रही हो, तो लोगों को उसमें कोई नुकसान नहीं दिखता है।
इस कमरे के पीछे कोई विचार है, या उसका उनके जीवन से सीधा संबंध है, यह समझाना आसान नहीं होता। सरकार के लिए तो यह बहुत मुश्किल होता है। सरकारी प्रचार और प्रसार वैसे भी उबाऊ होता है, पर-उपदेशों से अटा हुआ। फिर सरकारी प्रचार करने वालों का 'लाभार्थी' और हितग्राही लोगों के जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं होता।
कुछ गैरसरकारी संस्थाओं ने निर्मल भारत अभियान को अपनाकर कई गांवों में बेहतर काम कर के दिखाया है। इनमें ओडीशा की संस्था ग्राम विकास' का नाम भी आता है। ग्राम विकास का काम इस इलाके में पुराना है और यहां के गांवों से उसका संबंध भी रहा है। संस्था ने बीसियों गांवों के हर घर में शौचालय का इंतजाम किया है, उनके भीतर पानी का इंतजाम भी। इन गांवों में किसी को खुले में मलत्याग करना नहीं पड़ता। उनके प्रभाव वाले गांवों में जल संचय और वितरण की व्यवस्था भी होती है। इस काम की तारीफ करने वाले भी कहते हैं कि उनकी सफलता उनके इलाके तक ही सीमित है। अगर १,००० गांवों में भी हो तो फिर भी ओडीशा में तो कोई ५०,००० गांव हैं। वहां शुचिता का काम कैसे हो सकता है? सरकार की समस्या गैरसरकारी संस्थाओं से कहीं ज्यादा बड़ी है।
ग्राम विकास के अच्छे शौचालय बनाने में अनुदान भी काफी लगता है। संस्था के निदेशक जो मडियथ का कहना है कि यह मानसिकता ही गलत है कि गरीब लोगों के लिए होने वाला काम सस्ता और हल्का होना चाहिए। लेकिन सरकार द्वारा 'टोटल सैनिटेशन' को 'निर्मल भारत' में बदलने का एक कारण था सरकारी अनुदान की राशि घटाना, क्योंकि उससे शुचिता का काम हो नहीं रहा था। सरकार अगर किसी एक संस्था के अच्छे काम से सीखने को राजी हो भी जाए, फिर भी, वह उसकी तरह काम करे कैसे? उसे तो जिला प्रशासन, ग्राम पंचायतों और नगर निगमों के जरिए काम करना पड़ता है।
अनुदान से बने शौचालयों की कमजोरियां तो अब सरकार भी मानती है। इससे एक अंतर आया है सरकारी स्वच्छता अभियानों में। अब उनका प्रचार और प्रसार खूब जोर-शोर से होता है ताकि लोग खुद ,, अपने खर्चे से ही शौचालय बनाएं और उनका रखरखाव भी करें। इस बदलाव के पीछे कोलकाता में रहने वाले एक कृषि वैज्ञानिक का सन् १९९९ का एक तजुर्बा है। उनका नाम है कमल कार। वे एक गैरसरकारी संस्था के काम की समीक्षा करने के लिए बांग्लादेश के राजशाही जिले की यात्रा पर गए थे। वहां उन्हें चारों तरफ मल बिखरा मिला, जबकि वहां एक गैरसरकारी संस्था का शौचालय बनाने का कार्यक्रम चल रहा था। श्री कमल ने गांव के लोगों को खुद ही से शौचालय बनाने की बात की। जब लोगों ने उसका कारण पूछा तो श्री कमल ने उन्हें बहुत कडे और नाटकीय शब्दों में बताया कि घनी बस्ती में कई लोगों के खुले में मलत्याग करने से कैसे बीमारियां फैलती हैं। उन्होंने बार-बार कहा कि जाने-अनजाने, वे लोग एक-दूसरे का गू खा रहे थे।
उनके तीखे शब्द ग्रामीणों को तीर जैसे लगे। उनके मन में अपने व्यवहार के प्रति घिन पैदा हुई। कुछ लोगों ने तो वहीं कसम खाई कि वे शौचालय बनाएंगे और गांव से गंदगी दूर करेंगे। देखते-देखते पूरे गांव ने शौचालय बना लिए और अपना व्यवहार भी बदल लिया। बिना किसी सरकारी या गैरसरकारी अनुदान के । श्री कमल कहते हैं कि उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि गांव के लोगों में इतनी तेजी से बदलाव आया। इसके बाद वे दूसरे काम छोड़ कर शुचिता के काम में ही लग गए। बांग्लादेश में इसी तर्ज पर बहुत तेजी से काम हुआ। श्री कमल इसे एक समुदाय को 'ट्रिगर' करना कहते हैं, जैसे कि किसी बंदूक का घोडा दबा दिया हो। उसके बाद जैसे गोली अपना काम करती है ठीक वैसे ही समुदाय के लोग खुद शौचालय बनाते हैं और दूसरों पर दबाव डालते हैं कि वे भी ऐसा ही करें।
आगे चल के यह एक पद्धति ही बन गई। अंग्रेजी में इसका नाम पड़ा 'कम्यूनिटी लेड टोटल सैनिटेशन', या सी.एल.टी.एस.। यानी संपूर्ण स्वच्छता का ऐसा काम जो ध_ समुदाय के लोग अपने आप ही करें। सरकार और गैरसरकारी संस्थाएं लोगों की आंखें खोलने का काम भर करें, ताकि अपने व्यवहार के प्रति लोग शर्म महसूस करें, ' दर से घिन करना सीखें। फिर वे मलत्याग करने के ऐसे तरीके अपनाएं जिनमें इज्जत भी हो और वहां रहने वालों की सेहत भी ठीक रहे। इस पद्वति में लोग अपना शौचालय कैसा बनाएं यह उन्हें खुद तय करना होता है। श्री कमल का कहना है कि एक बार लोग शौचालय का इस्तेमाल करने के आदी हो जाएं तो वे धीरे-धीरे अच्छे शौचालय भी खुद ही बना लेते हैं। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं ने सी.एल.टी.एस. पद्वति को खूब बढ़ावा दिया है। आज ५० से ज्यादा देशों में इसी तर्ज पर काम हो रहा है, खासकर अफ्रीका में। कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए श्री कमल ने साहित्य तैयार किया है। इसमें ग्रामीणों को बहुत ही नाटकीय तरीके से खुले में मलत्याग के नुकसान बताए जाते हैं। लोगों का मन झकझोरा जाता है, उनमें शर्म और घिन पैदा करने के लिए। स्वच्छता पर होने वाली अंतर्राष्टीय बैठकों में सरकारी और गैरसरकारी कार्यकर्ता खुलेआम चर्चा करते हैं कि लोगों को शर्मिंदा करने के सबसे कारगर तरीके क्या हैं। कौन सा 'ट्रिगर' अचूक है। हमारी सरकार को सी.एल.टी.एस. अपनाने में समय लगा, हालांकि सन् २००३ में ही महाराष्ट्र सरकार के एक सचिव ने इसका प्रयोग किया था। इससे नानदेड़ और अहमदनगर में खुले में मलत्याग बंद हो गया था। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास कल्याणी पहला शहरी इलाका घोषित हुआ जो खुले में मलत्याग से मुक्त था। लेकिन श्री कमल यह मानते हैं कि भारत में सी.एल.टी.एस. पद्वति पर काम करना सरल नहीं है, क्योंकि सरकारी अनुदान लोगों को आलसी बनाता है। उनकी राय है कि एक बार कोई ग्रामीण समाज जाग जाए तो वह अपनी शुचिता का इंतजाम खुद करता है, लेकिन अनुदान मिलने की स्थिति में लोग इसे सरकार का काम मानते हैं। कुछ प्रांतीय सरकारों ने सी.एल.टी.एस. पद्वति को अपनाया है। हिमाचल प्रदेश इनमें सबसे आगे कहा जाता है। कई लोग मानते हैं कि सरकारी प्रचार तंत्र को कारगर बनाने का तरीका इसके सिवा कोई है ही नहीं। उन्हें यही सबसे कारगर तरीका लगता है गंदगी में रहने वाले लोगों के प्रबोधन का, उनके व्यवहार को बदलने का। शर्म और घृणा से लोगों को स्वच्छता और गरिमा दिलाने वाली इस पद्वति का आजकल बहुत बोलबाला है विकास की दुनिया में। इसमें सरकार का खर्च भी ज्यादा नहीं होता।
इस पद्वति का एक और पहलू है जिसकी चर्चा कम होती है। लोगों को शौचालय बनाने और इस्तेमाल करने के लिए राजी करने के तरीके हमेशा शिष्ट और सामाजिक नहीं होते। इनकी शुरुआत ही लोगों को शमिंदा करने से होती है और जगहों फिर है"
भयानक तरीके भी इस्तेमाल होते हैं। शिक्षकों और छात्रों के दल उन जगहों पर जाते हैं जहां लोग खुले में मलत्याग करने बैठते हैं। अगर कोई खुले में 'बैठा दिख. खुले आम _ सीटियां बजाई जाती हैं, उन पर पत्थर फेंकने के किस्से भी सुनने में आते हैं। खुले में शौच जाने वालों की तस्वीरें दीवारों पर चिपका कर उन्हें बेइज्जत करने जैसे तरीके भी इसमें शामिल हैं। कक्षा में उन छात्रों का अपमान किया जाता है जिनके यहां शौचालय नहीं होता। ऐसा करने वाले लोगों में दूसरों के प्रति करुणा भाव रत्ती भर नहीं होता। उल्टा वे उन्हें अपराधी मानते हैं और उनके प्रति बदले का भाव रखते हैं।
लोग जहां खुले में मलत्याग करने के आदी हों उन जगहों पर कार्यकर्ता पहले से खड्डे मिलते हैं, उन्हें रोकने के लिए। जब तक लोग शौचालय बनाने का अनुबंध न करें, ग्राम पंचायत पानी-बिजली काटने की धमकी तक दे देती है। एक अखबार की रपट तो यह भी बताती है कि कुछ गरीब लोगों की जमीन पर जबरदस्ती शौचालय बनाए गए, उनसे बिना पूछे। एक अधिकारी ने एक महिला का मल ले जा कर उसकी रसोई में पटक दिया। कुछ लोग जब दिशा-मैदान गए हुए थे तब पीछे से उनके घर पर ताला लगा दिया गया। जब वे चाभी लेने आए तो उन्हें पहले एक अनुबंध पर दस्तखत करना पड़ा कि वे शौचालय बनाएंगे। जिस स्वच्छता अभियान को मोहनदास गांधी के नाम पर, उनके चश्मे के चिह्र में चलाया जा रहा है, वह सामाजिक संबंधों को ऐसी हिंसक आंखों से कैसे देखता है?
हर कहीं ऐसी ही जोर-जबरदस्ती हुई हो ऐसा नहीं है। न ही सी.एल.टी.एस. के अनुभव सब जगह बुरे हैं। पर यह पूछना वाजिब है: क्या भारत को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए ऐसे साधन हमें स्वीकार्य हैं? इस तरह किया काम कब तक टिकेगा?
यह अभियान और इसके कार्यक्रम हमेशा नहीं चलेंगे। योजना निपटने के बाद क्या लोग वापस खुले में मलत्याग करने नहीं जाने लगेंगे, खासकर जब शौचालयों की देखरेख ठीक न हो और उनमें पानी न हो? इस पर बातचीत नहीं हो रही है अभी, क्योंकि शौचालय बनाने की होड़ चल रही है।
सी.एल.टी.एस. के समर्थकों का कहना है कि इसमें गलती सरकारी कार्यक्रमों में है, इस पद्बति में नहीं। उनका कहना है कि ठीक से काम हो तो समुदाय उन लोगों को राजी कर सकता है जो शौचालय बनाना नहीं चाहते। आखिर खुले में मलत्याग करने से पूरे समुदाय की सेहत पर असर पड़ता है, इसलिए समुदाय को ही उन लोगों को मनाना चाहिए जिनसे यह खतरा है। लेकिन सरकारी कार्यक्रमों में यह सब आसान नहीं होता है। उनके तरीके आदेशों के सीधे पालन के लिए बनते हैं। इतनी बारीकी की जगह नहीं होती है उनमें। इसे जितनी बार भी कहा जाए कम है: शुचिता केवल तकनीकी या इंजीनियरी का मामला नहीं है। शुचिता के मायने कई हैं, कई पेंच भी हैं इस विचार में। स्वच्छता की बात जिस भाषा में होती है वह हमारे जीवन में शुचिता के मायने ठीक से बता नहीं पाती। मलत्याग करना शरीर का ऐसा धर्म है जिसका इशारा भी सभ्य समाज में अटपटा माना जाता है। हर रोज मलत्याग करने की जरूरत हमें याद दिलाती है कि मनुष्य भी प्रकृति के बनाए कई प्राणियों में से एक है। राजा हो या रंक, कपड़े खोल जब कोई मनुष्य मलत्याग करने बैठता है तो सभ्यता और सांस्कृतिक विकास की धारणाएं फीकी पड़ जाती हैं।
पौराणिक कथाओं में खुद भगवान विष्णु ने वराहावतार में सूअर का रूप धारण किया था, लेकिन सभ्य भाषा में मलत्याग के दैनिक कर्म के लिए सीधे शब्द नहीं हैं। जैसे फारसी से आया शब्द 'पाखाना', जिसका अर्थ है 'षैर का घर'। या हिंदी का ही शब्द लीजिए, 'टट्टी'। इसका माने है कोई पर्दा या आड़ जो किसी फसल की ढूंठ, या टटिया से बनी हो। आज भी खुले में शौच जाने को कहते हैं दिशा-मैदान जाना। 'आब' को 'पेश' करने से बना शब्द 'पेशाब' तो फिर भी सीधा है, लेकिन 'लघु शंका' और 'दीर्घ शंका' जैसे शब्द अर्थ कम बताते हैं, संदेह ज्यादा पैदा करते हैं। मलत्याग करने के लिए जो 'हगना' और 'चिरकना' जैसा सीधे, क्रिया-रूपी शब्द हैं उनका उपयोग पढे-लिखे समाज में बुरा माना जाता हैं। इन शब्दों के साथ घृणा जुड़ी हुई है।
घृणा एक तीव्र, सर्वव्यापी, जन्मजात भावना है। इसकी अभिव्यक्ति हम सब जानते हैं। चेहरे पर रेखाएं खिंचती हैं, नाक-भी सिकुड़ती है, मुंह के किनारे नीचे की ओर मुड़ते हैं, रक्तचाप गिरता है, मितली होने का भाव चेहरे पर आ जाता है। प्राचीन काल में भरत मुनि के रचे ग्रंथ 'नाट्यशास्त्र' में बताए रसों में एक है वीभत्स रस। यानी जुगुप्सा, या घृणा, या घिन। शिव इस रस के ईष्ट देव हैं। आज भी रंगमंच की शिक्षा में सिखाए जाने वाले भाव में वीभत्स रस मूल है, फिर चाहे वह भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से हो या अभिनय की किसी आधुनिक फिल्मी विधा से।
कई तरह के वैज्ञानिकों ने घृणा को समझने की कोशिश की है। अनेक शोध और सर्वेक्षणों में इस भाव का सबसे ताकतवर स्रोत हमारा मल ही निकला है। घृणा किसीन-किसी रूप में हर मनुष्य में होती है, हालांकि इसकी अभिव्यक्ति संस्कार से है। हमारे यहां मनुष्य का मल घृणा का पात्र है पर गाय-बैल का गोबर नहीं, बल्कि इनका गोबर तो पवित्र माना गया है। कुछ समाजों में सूअर जैसे मल खाने वाले पशु को अशुद्व और असहनीय माना है, जबकि ऐसे समाज भी हैं जो इन्हें स्वीकार करते हैं और पास रखते हैं।
ज्ञान-विज्ञान की दुनिया के कई प्रसिद्घ नामों ने घृणा पर अपने बिच जीव-वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने इसे मनुष्य की छह मूल भावनाओं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्राएड मल के प्रति घिन को मानते थे। शिशुओं को अपने मल से घृणा नहीं होती, मल् से निकले पदार्थों के प्रति कुतूहल और आकर्षण का भाव रहता होता है तब उसे परिवार और समाज सिखलाता है कि मल घृणित वस्तु है। आजकल कुछ वैज्ञानिक इससे ठीक उल्टा मानते हैं, वे कहते हैं कि घृणा का भाव जन्मजात है। इसकी अभिव्यक्ति दो से पांच साल की उम्र में शुरू होती है और इसकी कम-से-कम एक खास वजह तो है ही। यह प्रकृति का तरीका है हमें उन चीजों से दूर रखने का जिनसे हम बीमार हो सकते हैं। रोगाणुओं के सबसे ताकतवर स्रोतों में हमारा अपना मल आता है। कई बीमारियां मल से ही फैलती हैं।
हमारा बचाव इसी में है कि हम अपने मल से तब तक दूर रहें जब तक उसमें मौजूद रोगाणु खत्म नहीं हो जाते। उसे हमारे लिए बदबूदार बन देना प्रकृति का तरीका है हमें उससे दूर रखने का। मल से जो गंध आती है उसमें सडे अंडे और गंधक का संकेत होता है। यह हर रूप में मनुष्य मात्र को अप्रिय है। शायद इसीलिए न जाने कब से मनुष्य सहज ही मलत्याग करने बस्ती से थोड़ा दूर जाता है। शुचिता का बुनियादी पैमाना यही रहा है कि मनुष्य अपने मल से दूर ही रहे। मनुष्य का सबसे प्रिय मित्र कहा जाने वाला कुत्ता तो मलत्याग करने के बाद अपने पैर से जमीन खोद कर उस पर मिट्टी बिखेर देता है। हर संस्कृति, हर समाज में यह बोध किसी-न-किसी रूप में रहा है। हर समाज में शुचिता को ले कर तरह-तरह के रिवाज रहे हैं। लोग जिन रिवाजों में बड़े होते हैं वही उन्हें शुचिता और स्वच्छता का मानक लगते हैं। दूसरे लोगों के साफ रहने के तरीके लोगों को उतने जमते नहीं हैं, क्योंकि शुचिता के व्यवहार का घृणा से गहरा संबंध है। हम जिन्हें अपना मानते हैं उन्हें साफ- सुथरा समझते हैं। जिन्हें अपना नहीं मानते, उनकी आदतें भी गंदी ही दिखती हैं। यह मानव स्वभाव है। किसी मां को अपने शिशु के गंदे पोतडों से घिन नहीं आती, और आती भी है तो वह उसे सहन करना सीख लेती है। शोध बतलाता है कि माताओं को दूसरों के शिशुओं के पोतडे इतने साफ नहीं लगते जितने अपने शिशु के लगते हैं।
शुचिता और घृणा का व्यवहार केवल व्यक्तिगत नहीं होता है। सामाजिकता में भी यह झलकता है। शुचिता और घृणा का संबंध सामाजिक संरचना से भी रहा है। अपने वर्ग या समाज या धर्म या जाति के लोगों को साफ मानना और दूसरों को गंदा मानना भी मनुष्य स्वभाव का हिस्सा रहा है। जिन संस्कृतियों में मलत्याग करने के बाद गुदा को पानी से धोने का रिवाज है वे उन लोगों को गंदा मानते हैं जो कागज से पोंछते हैं। कागज से पोंछने वालों से अगर आप पूछे तो सुनने को मिलेगा कि पानी से धोना बहुत झंझट भरा, बेवजह और अस्वच्छ व्यवहार है। ये आदतें धार्मिंक ग्रंथों और रिवाजों में भी गुंथी हुई हैं। धार्मिक संस्कार और शुचिता का संबंध इतना पुराना है कि यह कहना कठिन है कि उसका कौन सा हिस्सा धार्मिक रूढि से निकला है, और कौन सा हिस्सा व्यावहारिक शुचिता से। एक धर्म के लोगों का व्यवहार भी जगह और समय के हिसाब से बदलता रहा है।
एक उदाहरण है ऐसे तीन धर्मों का जो अपनी व्युत्पत्ति हजरत इब्राहिम से मानते हैं। यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म, तीनों ही अपने आप को इब्राहिमी कहते हैं। इब्राहिम का वृत्तांत बाइबल के 'ओल्ड टेस्टामेंट' में मिलता है। इसके पांचवें अध्याय में उस समय के घुमंतू लोगों के लिए शौच जाने के नियम दिए हुए हैं, जिसमें बस्ती से दूर जा कर, जमीन में गड्ढा कर के, उसमें मलत्याग करने की बात आती है। इसके बाद मल पर मिट्टी डालने का निर्देश भी है। इस्लाम में 'वुजू' का कायदा है, जिसमें नमाज के पहले शुद्घ होने के तरीके बतलाए गए हैं। हिंदू रिवाजों में मलत्याग करने के बाद नहाने का वर्णन मिलता है। कई हिंदू और मुस्लिम समाजों में मलत्याग करने के बाद गुदा पानी से धोने का रिवाज रहा है। यह बाएं हाथ से ही किया जाता है क्योंकि दाहिना हाथ कई 'शुद्घ' माने जाने वाले कामों के लिए आरक्षित होता है। हिंदू पूजाओं में बाएं हाथ का उपयोग बहुत सी जगह वर्जित है, जैसे तिलक कभी बाएं हाथ से नहीं लगाया जाता, अग्नि में होम केवल दाहिने हाथ से ही दिया जाता है। कई मुस्लिम समाजों में खाने-पीने की चीज बाएं हाथ से देना ऐब माना जाता है। धार्मिक रीति में डाली हुई बातें बहुत लंबी चलती हैं। ये रिवाज जब बने थे तब ज्यादातर लोग गांवों में रहते थे और शौच जाने के लिए ढेर सारी जमीन थी।
पर हमारी दुनिया पिछली शताब्दी में बहुत तेजी से बदली है। मनुष्य की कुल आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा अब शहरों में रहता है। जिन रीति-रिवाजों से लोग पहले शचिता और पवित्रता अपनी-अपनी तरह बनाए रखते थे उनमें से कई तो आज बेतुके हो चुके हैं, या उन्हें आज की जरूरतों के हिसाब से ढालने की जरूरत है। लेकिन सामाजिक व्यवहार इतनी तेजी से बदलता नहीं है। हर वर्ग, हर समाज के लोग अपने रिवाजों में रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका सामाजिक जीवन उन रिवाजों के इर्दगिर्द ही बनता है। चाहे अच्छे हों या बुरे, ये रिवाज कोई एक दिन में नहीं बनते। इसलिए आ कर कहे कि आपके व्यवहार से आप ही नहीं, आपके पडोसियों को खतरे में पड़ता है, तो लोगों का मन इतनी आसानी से बदलता नहीं है। तब तो और भी नहीं जब उन्हें ये बातें समझाने वाले व्यक्ति का उनके जीवन से कोई लेना-देना हो ही नहीं, जिसका उनसे एकमात्र संबंध उनके मलत्याग करने की जगह से हो। ऐसा भी देखने में आता है कि लोगों को यह समझ नहीं आता कि जिन सरकारी अफसरों और संभ्रांत लोगों को उनकी दूसरी समस्याओं से कोई मतलब नहीं होता, वे उनके लिए शौचालय बनाने की इतनी चिंता क्यों करते हैं। अगर लोग बदल भी जाएं तो क्या केवल खुले में शौच जाना रुकने से शुचिता आ जाएगी? क्या शौचालय बनाना और इस्तेमाल करना ही संपूर्ण समाधान है? अगर हर किसी के पास सीवर का शौचालय होगा तो हमारे जल स्रोतों का क्या होगा?
सरकारी स्वच्छता अभियानों में आग्रह शर्म का है, विवेक का नहीं। हमारी सरकार ही नहीं, पढे-लिखे समाज को अपने देश के उन लोगों की वजह से शर्म आती है जो खुले में शौच जाते हैं। अपनी नदियों और तालाबों को सीवर बना डालने में कोई शर्म नहीं आती। हमारी सरकारें जिन शहरों में बैठती हैं उनका पानी दूर के गांवों से छीन कर लाया जाता है। जब अपने जल स्रोतों की जरूरत कम हो जाती है तो उन्हें साफ करना एक थोथा आदर्श बन कर रह जाता है, जो 'गंगा ऐक्शन प्लैन' जैसे सुनने में अच्छे पर वास्तव में एकदम बेअसर कार्यक्रमों में तब्दील हो जाता है। इस नजरिए से देखें तो सीवर से जुड़े शौचालय पर्यावरण के प्रदूषण के सबसे खतरनाक स्रोत हैं। शुचिता का विचार सीधा-सरल नहीं है। इसे समझना हो तो किसी सफाई कर्मचारी से जिसे अपने हाथ से दूसरों का मल- मूत्र साफ करना पड़ता है। हमारे कई शहरों में आज भी हाथ से मैला साफ करवाया जाता है, चाहे वह भारतीय रेल हो जिसमें पटरियों को साफ करने के लिए सफाई कर्मचारी रखे जाते हैं, या सूखे शौचालय वाली शहरी बस्तियां हों। यह काम कुछ खास जाति के लोगों से ही करवाया जाता है। रुकी हुई सीवर की नालियां खोलने के लिए भी इन्हीं जातियों के सफाई कर्मचारी उनके भीतर डुबकी लगाते हैं। ऐसा करते हुए हर साल कई कर्मचारियों की जान जाती है। सीवर की सफाई के लिए कई लोगों की बलि चढा दी जाती है।
यह है घृणा का राजनीतिशास्त्र।
--
(साभार - जल थल मल, गांधी शांति प्रतिष्ठान)




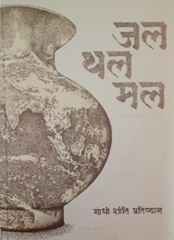
रचना बहुत अच्छी है परंतु त्रुटियों से भरपूर है और इस के बहुत सशक्त सम्पादन के बिना पोस्ट किये जाने पर आपत्ति है . इस से रचनाकार
जवाब देंहटाएंकी क्रेडिबिलिटी प्रभावित होती है. बाकी प्रकाशकों की मर्जी है .
स्वराज सेनानी जी,
जवाब देंहटाएंआपकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद। कृपया थोड़ा विस्तार से बताएं कि कैसी व किस तरह की त्रुटियाँ हैं। इस आलेख को किताब से स्कैन कर डिजिटाइज किया गया है, अतः संभवतः कुछ अवांछित त्रुटियाँ घुस आईं हैं जिसके लिए खेद है। आशय यह है कि अच्छी जानकारी पाठकों तक पहुंचे।